
रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति, नागरिक जागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा
क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों में हो रहा है या उपभोग में?क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है? -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र
गोंदिया – वैश्विक स्तरपर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जहाँ 142.6 करोड़ से अधिक नागरिकों की आकांक्षाएँ, आवश्यकताएँ और अधिकार एक जटिल राजनीतिक-आर्थिक ढांचे के माध्यम से संचालित होते हैं। लोकतांत्रिक प्रतिस्पर्धा स्वाभाविक है,परंतु जब यह प्रतिस्पर्धा विकासात्मक दृष्टि के स्थान पर अल्पकालिक लोक लुभावन वादों में बदल जाती है,तब उसके दूरगामी परिणाम राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य और सामाजिक संरचना दोनों पर पड़ते हैं। हाल के वर्षों में चुनावी मौसम में मुफ्त सुविधाओं, बिजली,पानी,नकद हस्तांतरण, लैपटॉप साइकिल इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं,उपभोक्ता वस्तुएँ, परिवहन,उपकरण विद्यार्थी अनेक मुफ्त बांटने कीघोषणाओं ने रेवड़ी संस्कृति को एक प्रमुख राष्ट्रीय बहस का विषय बना दिया है। यह बहस केवल राजनीतिक विमर्श नहीं है,बल्कि संविधान,वित्तीय अनुशासन, करदाताओं के अधिकार और भावी पीढ़ियों की आर्थिकसुरक्षा से जुड़ा प्रश्न बन चुकी है।अभी फिर से एक बार गुरुवार दिनांक 19 फरवरी 2026 को भारत क़ी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ,सीजेआई सूर्यकांत,जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली ने तमिलनाडु विद्युत वितरण निगम के मामले की सुनवाई के दौरान मुफ्त बिजली की संस्कृति पर कठोर टिप्पणी की।अदालत ने स्पष्ट कहा कि उपभोक्ता क़ि वित्तीय स्थिति का परीक्षण किए बिना सार्वभौमिक रूप से मुफ्त बिजली देना राज्य के आर्थिक विकास को बाधित कर सकता है।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क़ि न्यायालय की यह टिप्पणी केवल एक राज्य तक सीमित नहीं थी;यह समग्र नीति-दृष्टि पर प्रश्नचिह्न था।अदालत ने इंगित किया कि जब राज्य पहले से ऋणग्रस्त हों और विकास परियोजनाओं के लिए संसाधन सीमित हों,तब खैरात आधारित राजनीति वित्तीय अनुशासन को कमजोर करती है और दीर्घकालीन बुनियादी निवेशों, जैसे आधारभूत संरचना,स्वास्थ्य शिक्षा को प्रभावित करती है। 21 जनवरी 2026 को भी शीर्ष न्यायालय ने इस विषय को अत्यंत महत्वपूर्ण करार देते हुए लंबित याचिकाओं की शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर बल दिया था। याचिकाकर्ता ने देश पर बढ़ते सार्वजनिक ऋण लगभग 250 लाख करोड़ रूपए की ओर ध्यान आकृष्ट किया। न्यायालय ने स्वीकार किया कि नीति-निर्णय का क्षेत्र कार्यपालिका का है,परंतु यह भी पूछा कि क्या राज्य के राजस्व का एक सुनिश्चित हिस्सा केवल विकास कार्यों के लिए सुरक्षित नहीं होना चाहिए? यह प्रश्न संघीय ढांचे के भीतर वित्तीय उत्तरदायित्व और जनहित के संतुलन का मूल प्रश्न है।
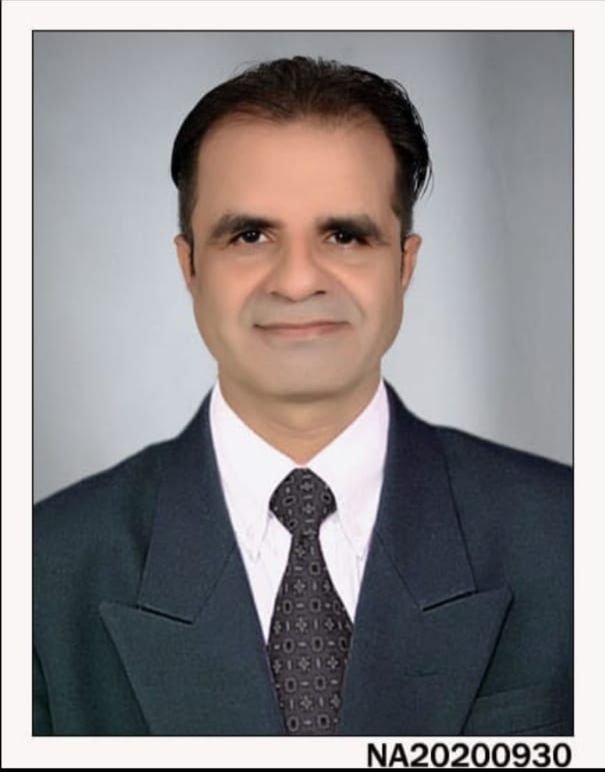
साथियों बात अगर हम न्यायालय की टिप्पणियों को गहराई से समझने की करें तो उसका एक केंद्रीय बिंदु था कल्याणकारी योजनाओं और चुनावी फ्रीबीज के बीच अंतर। संविधान के नीति निदेशक तत्व राज्य को शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपते हैं। यदि राज्य निर्धन या वंचित वर्गों को मुफ्त शिक्षा या स्वास्थ्य सुविधा देता है,तो वह संवैधानिक दायित्व का निर्वहन है। किंतु जब बिना लक्षित पहचान के, बिना वित्तीय क्षमता के आकलन के, व्यापक स्तरपर मुफ्त वस्तुओं का वितरण केवल चुनावी लाभ हेतु किया जाए,तब वह नीति-आधारित कल्याण नहीं बल्कि अल्पकालिक राजनीतिक निवेश प्रतीत होता है।अदालत ने रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने कीआवश्यकता रेखांकित करते हुए कहा कि उत्पादक क्षमता को बढ़ाने वाली नीतियाँ ही दीर्घकालीन समाधान हैं।
साथियों बात अगर हम आर्थिक दृष्टि इस मुद्दे को समझने की करें तो रेवड़ी संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव राजकोषीय घाटे और सार्वजनिक ऋण पर पड़ता है। राज्यों का बड़ा हिस्सा पहले ही वेतन,पेंशन और ब्याज भुगतान में खर्च हो जाता है।यदि अतिरिक्त संसाधन मुफ्त योजनाओं में लगाए जाते हैं, तो पूंजीगत व्यय सड़क,जल प्रबंधन,ऊर्जा ढांचा,औद्योगिक क्लस्टर के लिए संसाधन घटते हैं। इससे रोजगार सृजन की गति धीमी होती है और कराधान का आधार भी सीमित रहता है। एक दुष्चक्र बनता है: कम निवेश कम उत्पादन, कम राजस्व,अधिक उधारी और अधिक लोकलुभावन घोषणाएँ। न्यायालय द्वारा परजीवी मानसिकता की आशंका इसी आर्थिक तर्क से जुड़ी है,यदि नागरिकों को उत्पादक अवसरों के स्थान पर अनुदान आधारित निर्भरता की ओर प्रेरित किया जाए, तो श्रम भागीदारी और नवाचार दोनों प्रभावित हो सकते हैं।
साथियों बात अगर हम लोकतांत्रिक विमर्श का एक अन्य पहलू चुनावी समानता और निष्पक्षता है इसकोसमझने की करें तो,यदि राजनीतिक दल करदाताओं के धन से भविष्य में दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं का वादा कर मतदाताओं को प्रभावित करते हैं,तो क्या यह चुनावी प्रतिस्पर्धा की नैतिक सीमा का उल्लंघन है? चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों में घोषणापत्रों की पारदर्शिता की बात कही गई है, परंतु उनके वित्तीय स्रोत और व्यावहारिकता का स्वतंत्र मूल्यांकन अनिवार्य नहीं है। इस संदर्भ में न्यायालय का यह संकेत महत्वपूर्ण है कि गंभीर मामलों को तीन न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा, ताकि व्यापक संवैधानिक प्रश्नों पर स्पष्टता आए।रेवड़ी संस्कृति का सामाजिक आयाम भी उतना ही महत्वपूर्ण है।भारत में ऐतिहासिक रूप से सामाजिक- आर्थिक असमानताएँ रही हैं। कल्याणकारी योजनाएँ सामाजिक न्याय का उपकरण रही हैं,मिड-डे मील,सार्वजनिक वितरण प्रणाली, छात्रवृत्ति, मनरेगा जैसे कार्यक्रमों ने गरीबी उन्मूलन में योगदान दिया है। इसलिए किसी भी बहस में यह सावधानी आवश्यक है कि वास्तविक कल्याणकारी योजनाओं को फ्रीबीज कहकर खारिज न किया जाए।न्यायालय ने भी शिक्षा और स्वास्थ्य को संवैधानिक दायित्व के रूप में स्पष्ट किया।इसलिए मूल प्रश्न यह है कि लक्षित, आवश्यकता -आधारित, पारदर्शी और वित्तीय रूप से टिकाऊ योजनाओं और सार्वभौमिक,अस्थायी, चुनावी लाभ वाली योजनाओं के बीच रेखा कैसे खींची जाए।यदि इस प्रवृत्ति को नियंत्रित करने हेतु कठोर कानून बनाने की बात हो, तो उसका उद्देश्य प्रतिबंध मात्र नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करना होना चाहिए। संभावित कानून का नाम हो सकता है,राष्ट्रीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं चुनावी लोकलुभावन व्यय विनियमन अधिनियम। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक चुनावी घोषणा के लिए अनिवार्य वित्तीय स्रोत-प्रमाणन,स्वतंत्र आर्थिक मूल्यांकन और दीर्घकालिक प्रभाव विश्लेषण की व्यवस्था की जा सकती है। एक स्वतंत्र चुनावी व्यय एवं लोकलुभावन नीति मूल्यांकन आयोग गठित किया जा सकता है, जो घोषणापत्रों की व्यवहार्यता पर सार्वजनिक रिपोर्ट जारी करे। साथ ही, राज्य के बजट का एक न्यूनतम प्रतिशत पूंजीगत व्यय हेतु सुरक्षित रखने का संवैधानिक प्रावधान भी किया जा सकता है।साथ ही यह भी आवश्यक है कि पारदर्शिता को बढ़ाया जाए। यदि कोई राज्य मुफ्त बिजली देना चाहता है,तो उसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि उसका वित्तीय स्रोत क्या है, कितनी अवधि तक योजना चलेगी,और उसका ऋण- जीडीपी अनुपात पर क्या प्रभाव पड़ेगा।संसद और विधान सभाओं में पूर्व- अनुमोदन और सार्वजनिक विमर्श की बाध्यता लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व को सुदृढ़ करेगी।न्यायालय का हस्तक्षेप नीति-निर्माण में प्रत्यक्ष दखल नहीं बल्कि संवैधानिक मर्यादा की तत्परता से याद दिलाना है।

साथियों बात अगर हम इस मुद्दे पर एक सख्त कानून बनाए जाने की करें तो मेरा सुझाव है क़ि भारत में चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा रेवड़ियां (मुफ़्त उपहार, नकद लाभ, वादों के रूप में प्रत्यक्ष प्रलोभन) बाँटने का मुद्दा अक्सर लोकतांत्रिक नैतिकता और वित्तीय अनुशासन से जोड़ा जाता है। इस संदर्भ में यदि अत्यंत सख्त और निवारक कानून की परिकल्पना की जाए, तो वें प्रभावशाली,स्पष्ट और दंडात्मक भावना वाले होने चाहिए। मेरे विचार से संभावित कठोर विधेयक/अधिनियम नाम सुझाए जा रहे हैं(1)लोकतांत्रिक शुचिता एवं चुनावी प्रलोभन निषेध अधिनियम, 2026 (2) चुनावी रेवड़ी उन्मूलन एवं कठोर दंड अधिनियम, 2026 (3) राजकोषीय अनुशासन एवं लोकलुभावन वादा नियंत्रण अधिनियम, 2026(4)चुनाव प्रलोभन अपराध नियंत्रण एवं दंड संहिता अधिनियम, 2026 (5) राजनीतिक वित्तीय पारदर्शिता एवं मुफ्त वितरण प्रतिबंध अधिनियम, 2026 (6) जनमत प्रलोभन निषेध एवं लोकधन संरक्षण अधिनियम, 2026(7) चुनावी लोकलुभावन घोषणापत्र विनियमन एवं दंड अधिनियम, 2026(8)लोकतंत्र संरक्षण (अवैध चुनावी लाभ वितरण निषेध) अधिनियम, 2026 (9) राजनीतिक जवाबदेही एवं अनुदान दुरुपयोग निवारण अधिनियम, 2026 (10) चुनावी भ्रष्ट आचरण (मुफ्त वस्तु/नकद प्रलोभन) पूर्ण प्रतिबंध अधिनियम, 2026
साथियों बात अगर हम इस मुद्दे को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो भी यह प्रश्न नया नहीं है। कई लोकतांत्रिक देशों में चुनावी वादों की सीमा तय करने के लिए राजकोषीय नियम बनाए गए हैं। यूरोपीय संघ में सदस्य देशों पर घाटे और ऋण की सीमा संबंधी मानक लागू हैं। लैटिन अमेरिकी देशों ने अतीत में लोकलुभावन व्यय के कारण आर्थिक संकट झेले हैं, जहाँ अत्यधिक सब्सिडी और मुफ्त वितरण ने मुद्रास्फीति और मुद्रा अवमूल्यन को जन्म दिया। भारत जैसे उभरते अर्थतंत्र के लिए यह चेतावनी है कि अल्पकालिक राजनीतिक लाभ दीर्घकालिक आर्थिक अस्थिरता का कारण न बन जाए।
अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि प्रश्न यह नहीं कि कल्याणकारी राज्य होना चाहिए या नहीं, भारत का संविधान स्वयं एक कल्याणकारी राज्य की परिकल्पना करता है। प्रश्न यह है कि क्या कल्याण दीर्घकालिक सशक्तिकरण की दिशा में है या अल्पकालिक निर्भरता की ओर? क्या संसाधनों का उपयोग उत्पादक परिसंपत्तियों में हो रहा है या उपभोग में?क्या करदाताओं के धन का उपयोग पारदर्शी और न्यायसंगत है? और क्या भविष्य की पीढ़ियों पर ऋण का बोझ अनावश्यक रूप से डाला जा रहा है?न्यायपालिका की हालिया टिप्पणियाँ इस बहस को एक नई गंभीरता प्रदान करती हैं।यदि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका मिलकर एक संतुलित ढांचा विकसित करें जहाँ सामाजिक न्याय,आर्थिक अनुशासन और लोकतांत्रिक नैतिकता का समन्वय हो तो भारत न केवल अपनी राजकोषीय स्थिरता को सुरक्षित रख सकेगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर एक उत्तरदायी लोकतंत्र का उदाहरण भी प्रस्तुत करेगा। रेवड़ी संस्कृति पर नियंत्रण केवल कानून का विषय नहीं,बल्कि राजनीतिक इच्छाशक्ति,नागरिकजागरूकता और आर्थिक विवेक का सम्मिलित परिणाम होगा। यही संतुलन भारत को सशक्त, आत्मनिर्भर और दीर्घकालिक विकास की दिशा में अग्रसर कर सकता है।
-संकलनकर्ता लेखक – क़र विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र 9284141425





